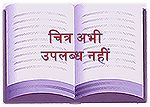"गीतिका -सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'" के अवतरणों में अंतर
गोविन्द राम (चर्चा | योगदान) छो (गीतिका -निराला का नाम बदलकर गीतिका -सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' कर दिया गया है) |
गोविन्द राम (चर्चा | योगदान) |
||
| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
| − | + | {{सूचना बक्सा पुस्तक | |
| − | + | |चित्र=Blank-image-book.jpg | |
| + | |चित्र का नाम= | ||
| + | |लेखक= [[सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला']] | ||
| + | |कवि= | ||
| + | |मूल शीर्षक = गीतिका | ||
| + | |मुख्य पात्र = | ||
| + | |कथानक = | ||
| + | |अनुवादक = | ||
| + | |संपादक = | ||
| + | |प्रकाशक = | ||
| + | |प्रकाशन_तिथि = [[1936]] ई. | ||
| + | |भाषा = [[हिंदी]] | ||
| + | |देश = [[भारत]] | ||
| + | |विषय = | ||
| + | |शैली = | ||
| + | |मुखपृष्ठ_रचना = | ||
| + | |विधा = [[काव्य संग्रह|काव्य-संग्रह]] | ||
| + | |प्रकार = | ||
| + | |पृष्ठ = | ||
| + | |ISBN = | ||
| + | |भाग = | ||
| + | |विशेष = इसके गीतों को संगीतात्मक बनाने के लिए शब्द ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया गया है। | ||
| + | |टिप्पणियाँ = | ||
| + | }} | ||
| + | '''गीतिका''' का प्रकाशन-काल सन् 1936 ई. है। इसमें [[सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला']] के नये स्वर-तालयुक्त शास्त्रानुमोदित गीत संगृहित हैं। [[खड़ी बोली]] में इस प्रकार के प्रथम गीत-रचनाकार [[जयशंकर प्रसाद]] हैं। उनके नाटकों के अंतर्गत जिन गीतों की सृष्टि हुई है, वे सर्वथा शास्त्रानुमोदित हैं किंतु ये गीत विशेष वातावरण में उनके पात्रों द्वारा गाये जाते है। ये गीत पात्र तथा वातावरण सापेक्ष हैं। शास्त्रानुमोदित निरपेक्ष गीतों की सर्जना का श्रेय 'निराला' को ही है। शास्त्रानुमोदित का तात्पर्य यह नहीं कि ये गीत भी पुरानी राग-रागनियों के बंधनों से बँधे हुए हैं। [[बंगाल]] में रहने के कारण 'निराला' का ध्यान बंगाल के उन गीतों की ओर गया जिनकी स्वर-लिपियाँ [[अंग्रेज़ी]] संगीत के आधार पर तैयार की गयी थीं। किंतु [[बांग्ला भाषा|बंगला]] में अंग्रेज़ी स्वर-शैली की हूबहू नकल नहीं की गयी। 'गीतिका' की भूमिका में 'निराला' ने स्वयं लिखा है- <blockquote>अंग्रेज़ी संगीत की पूरी नकल करने से पर उससे भारत के कानों को कभी तृप्ति होगी, यह संदिग्ध है। कारण, भारतीय संगीत की स्वर-मैत्री में जो स्वर प्रतिकूल समझे जाते हैं, वे अंग्रेज़ी संगीत में लगते हैं।"...</blockquote> | ||
| + | ==संगीत और काव्य== | ||
संगीत और काव्य में जहाँ विशेष संबंध है, वहाँ इनका अंतर भी स्पष्ट है। [[संगीत]] में स्वर की प्रधानता होती है और यह अपेक्षा कृत अपरिवर्तनशील कला है। संगीत के लिए काव्य अनिवार्य नहीं है, पर काव्य के लिए एक प्रकार के संगीत की अनिवार्यता मानी जा सकती है। 'गीतिका' में संगृहीत गीतों में संगीत-तत्व के साथ ही काव्य-तत्व का भी प्रचुर विनियोग हुआ है। इसमें कई प्रकार के गीत हैं- आत्मनिवेदन या प्रार्थनाप्रधान गीत, नारी सौंदर्य-चित्रणप्रधान, प्रकृति वर्णनपरक, दार्शनिक एवं राष्ट्रीय गीत। | संगीत और काव्य में जहाँ विशेष संबंध है, वहाँ इनका अंतर भी स्पष्ट है। [[संगीत]] में स्वर की प्रधानता होती है और यह अपेक्षा कृत अपरिवर्तनशील कला है। संगीत के लिए काव्य अनिवार्य नहीं है, पर काव्य के लिए एक प्रकार के संगीत की अनिवार्यता मानी जा सकती है। 'गीतिका' में संगृहीत गीतों में संगीत-तत्व के साथ ही काव्य-तत्व का भी प्रचुर विनियोग हुआ है। इसमें कई प्रकार के गीत हैं- आत्मनिवेदन या प्रार्थनाप्रधान गीत, नारी सौंदर्य-चित्रणप्रधान, प्रकृति वर्णनपरक, दार्शनिक एवं राष्ट्रीय गीत। | ||
| − | + | ==संगीतात्मकता== | |
इसके गीतों को संगीतात्मक बनाने के लिए शब्द ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यापक सांस्कृतिक परिवेश ग्रहण करने के कारण वे वस्तुमूलक, बौद्धिक तथा अधिक गूढ़ भावों के द्योतक हो गये। कहीं-कहीं लघुकाय गीतों में भाव अँट नहीं पाया है और कहीं-कहीं दुरूह शब्दयोजना प्रेषणीयता में विशेष बाधा डालती हुई दीख पड़ती है। किंतु ऐसे गीतों की संख्या अल्प है। | इसके गीतों को संगीतात्मक बनाने के लिए शब्द ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यापक सांस्कृतिक परिवेश ग्रहण करने के कारण वे वस्तुमूलक, बौद्धिक तथा अधिक गूढ़ भावों के द्योतक हो गये। कहीं-कहीं लघुकाय गीतों में भाव अँट नहीं पाया है और कहीं-कहीं दुरूह शब्दयोजना प्रेषणीयता में विशेष बाधा डालती हुई दीख पड़ती है। किंतु ऐसे गीतों की संख्या अल्प है। | ||
| − | {{लेख प्रगति|आधार= | + | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} |
| − | |||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
{{cite book | last =धीरेंद्र| first =वर्मा| title =हिंदी साहित्य कोश| edition =| publisher =| location =| language =हिंदी| pages =134| chapter =भाग- 2 पर आधारित}} | {{cite book | last =धीरेंद्र| first =वर्मा| title =हिंदी साहित्य कोश| edition =| publisher =| location =| language =हिंदी| pages =134| chapter =भाग- 2 पर आधारित}} | ||
==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||
| − | |||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
| − | + | {{आधुनिक साहित्यिक रचनाएँ}} | |
[[Category:साहित्य_कोश]] | [[Category:साहित्य_कोश]] | ||
[[Category:सूर्यकान्त_त्रिपाठी_निराला]] | [[Category:सूर्यकान्त_त्रिपाठी_निराला]] | ||
[[Category:काव्य कोश]] | [[Category:काव्य कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
13:23, 6 सितम्बर 2013 का अवतरण
गीतिका -सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'
| |
| लेखक | सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' |
| प्रकाशन तिथि | 1936 ई. |
| देश | भारत |
| भाषा | हिंदी |
| विधा | काव्य-संग्रह |
| विशेष | इसके गीतों को संगीतात्मक बनाने के लिए शब्द ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया गया है। |
गीतिका का प्रकाशन-काल सन् 1936 ई. है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' के नये स्वर-तालयुक्त शास्त्रानुमोदित गीत संगृहित हैं। खड़ी बोली में इस प्रकार के प्रथम गीत-रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। उनके नाटकों के अंतर्गत जिन गीतों की सृष्टि हुई है, वे सर्वथा शास्त्रानुमोदित हैं किंतु ये गीत विशेष वातावरण में उनके पात्रों द्वारा गाये जाते है। ये गीत पात्र तथा वातावरण सापेक्ष हैं। शास्त्रानुमोदित निरपेक्ष गीतों की सर्जना का श्रेय 'निराला' को ही है। शास्त्रानुमोदित का तात्पर्य यह नहीं कि ये गीत भी पुरानी राग-रागनियों के बंधनों से बँधे हुए हैं। बंगाल में रहने के कारण 'निराला' का ध्यान बंगाल के उन गीतों की ओर गया जिनकी स्वर-लिपियाँ अंग्रेज़ी संगीत के आधार पर तैयार की गयी थीं। किंतु बंगला में अंग्रेज़ी स्वर-शैली की हूबहू नकल नहीं की गयी। 'गीतिका' की भूमिका में 'निराला' ने स्वयं लिखा है-
अंग्रेज़ी संगीत की पूरी नकल करने से पर उससे भारत के कानों को कभी तृप्ति होगी, यह संदिग्ध है। कारण, भारतीय संगीत की स्वर-मैत्री में जो स्वर प्रतिकूल समझे जाते हैं, वे अंग्रेज़ी संगीत में लगते हैं।"...
संगीत और काव्य
संगीत और काव्य में जहाँ विशेष संबंध है, वहाँ इनका अंतर भी स्पष्ट है। संगीत में स्वर की प्रधानता होती है और यह अपेक्षा कृत अपरिवर्तनशील कला है। संगीत के लिए काव्य अनिवार्य नहीं है, पर काव्य के लिए एक प्रकार के संगीत की अनिवार्यता मानी जा सकती है। 'गीतिका' में संगृहीत गीतों में संगीत-तत्व के साथ ही काव्य-तत्व का भी प्रचुर विनियोग हुआ है। इसमें कई प्रकार के गीत हैं- आत्मनिवेदन या प्रार्थनाप्रधान गीत, नारी सौंदर्य-चित्रणप्रधान, प्रकृति वर्णनपरक, दार्शनिक एवं राष्ट्रीय गीत।
संगीतात्मकता
इसके गीतों को संगीतात्मक बनाने के लिए शब्द ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यापक सांस्कृतिक परिवेश ग्रहण करने के कारण वे वस्तुमूलक, बौद्धिक तथा अधिक गूढ़ भावों के द्योतक हो गये। कहीं-कहीं लघुकाय गीतों में भाव अँट नहीं पाया है और कहीं-कहीं दुरूह शब्दयोजना प्रेषणीयता में विशेष बाधा डालती हुई दीख पड़ती है। किंतु ऐसे गीतों की संख्या अल्प है।
|
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
धीरेंद्र, वर्मा “भाग- 2 पर आधारित”, हिंदी साहित्य कोश (हिंदी), 134।
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख